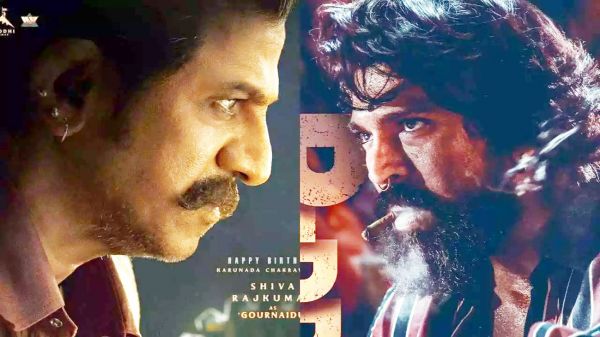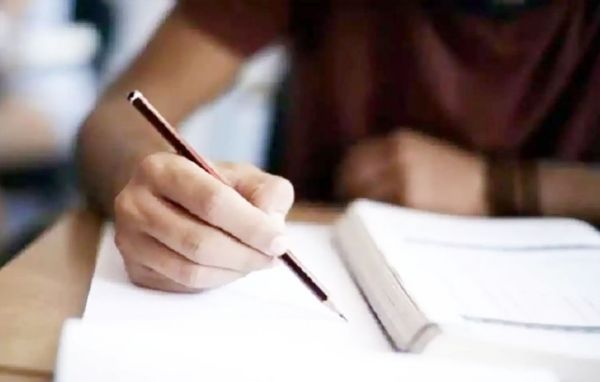संपादकीय डेस्क @झूठा-सच : काव्य के क्षेत्र में अपनी लेखनी से पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की भावना भर दी थी। राष्ट्रप्रेम की इस अजस्र धारा का प्रवाह बुंदेलखंड क्षेत्र के चिरगांव से कविता के माध्यम से हो रहा था। बाद में इस राष्ट्रप्रेम की इस धारा को देश भर में प्रवाहित किया था, राष्ट्रकविमैथिलीशरण गुप्त ने। इसलिए हिन्दी साहित्य जगत में 'दद्दा' नाम से सम्बोधित राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी को किया जाता था। बचपन में आप ने स्कूल में इनकी लिखी कविताएं जरूर पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी हैं तो आज हम आपको इस लेख से बताने वाले हैं कौन हैं राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त उनके लिखे रचनाएं।
मैथिलीशरण गुप्त जी स्वभाव से ही लोकसंग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे। उनका काव्य एक ओर वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी था। लाला लाजपतराय, बाल गंगाधर तिलक, विपिनचंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदनमोहन मालवीय उनके आदर्श रहे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पहले ही गुप्त का युवा मन गरम दल और तत्कालीन क्रान्तिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। 'अनघ' से पूर्व की रचनाओं में, विशेषकर जयद्रथ वध और भारत भारती में कवि का क्रान्तिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, राजेन्द्र प्रसाद, जवाहर लाल नेहरू और विनोबा भावे के सम्पर्क में आने के कारण वह गांधीवाद के व्यावहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलनों के समर्थक बने। 1936 में गांधी ने ही उन्हें मैथिली काव्य–मान ग्रन्थ भेंट करते हुए राष्ट्रकवि का सम्बोधन दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संसर्ग से गुप्तजी की काव्य–कला में निखार आया और उनकी रचनाएँ 'सरस्वती' में निरन्तर प्रकाशित होती रहीं। 1909 में उनका पहला काव्य जयद्रथ-वध आया। जयद्रथ-वध की लोकप्रियता ने उन्हें लेखन और प्रकाशन की प्रेरणा दी। 59 वर्षों में गुप्त जी ने गद्य, पद्य, नाटक, मौलिक तथा अनूदित सब मिलाकर, हिन्दी को लगभग 74 रचनाएँ प्रदान की हैं। जिनमें दो महाकाव्य, 20 खंड काव्य, 17 गीतिकाव्य, चार नाटक और गीतिनाट्य हैं।
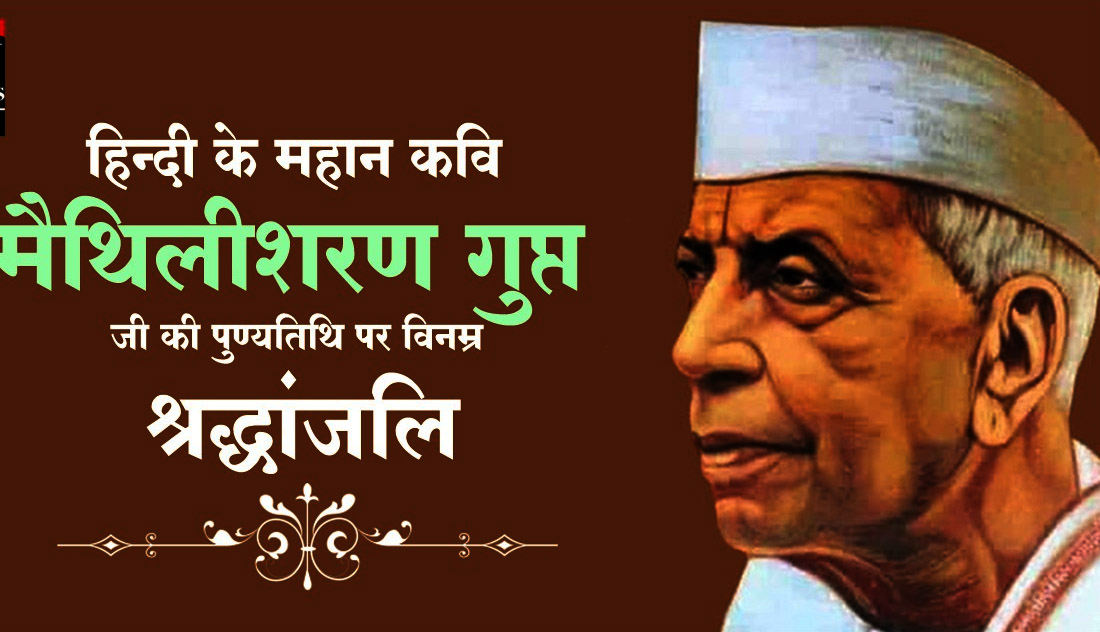
मैथिलीशरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगाँव, झाँसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। संभ्रांत वैश्य परिवार में जन्मे मैथिलीशरण गुप्त के पिता का नाम 'सेठ रामचरण' और माता का नाम 'श्रीमती काशीबाई' था। पिता रामचरण एक निष्ठावान् प्रसिद्ध राम भक्त थे। इनके पिता 'कनकलता' उप नाम से कविता किया करते थे और राम के विष्णुत्व में अटल आस्था रखते थे। गुप्त जी को कवित्व प्रतिभा और राम भक्ति पैतृक देन में मिली थी। वे बाल्यकाल में ही काव्य रचना करने लगे। पिता ने इनके एक छंद को पढ़कर आशीर्वाद दिया कि "तू आगे चलकर हमसे हज़ार गुनी अच्छी कविता करेगा" और यह आशीर्वाद अक्षरशः सत्य हुआ। उनके व्यक्तित्व में प्राचीन संस्कारों तथा आधुनिक विचारधारा दोनों का समन्वय था।
मैथिलीशरण गुप्त की प्रारम्भिक शिक्षा चिरगाँव, झाँसी के राजकीय विद्यालय में हुई। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त गुप्त जी झाँसी के मेकडॉनल हाईस्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए भेजे गए, पर वहाँ इनका मन न लगा और दो वर्ष बाद ही घर पर इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया । लेकिन पढ़ने की अपेक्षा इन्हें चकई फिराना और पतंग उड़ाना अधिक पसंद था। फिर भी इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिन्दी तथा बांग्ला साहित्य का व्यापक अध्ययन किया। इन्हें 'आल्हा' पढ़ने में भी बहुत आनंद आता था।
काव्य प्रतिभा
इसी बीच गुप्तजी मुंशी अजमेरी के संपर्क में आये और उनके प्रभाव से इनकी काव्य-प्रतिभा को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। अतः अब ये दोहे, छप्पयों में काव्य रचना करने लगे, जो कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) में प्रकाशित होने वाले 'वैश्योपकारक' पत्र में प्रकाशित हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जब झाँसी के रेलवे ऑफिस में चीफ़ क्लर्क थे, तब गुप्तजी अपने बड़े भाई के साथ उनसे मिलने गए और कालांतर में उन्हीं की छत्रछाया में मैथिलीशरण जी की काव्य प्रतिभा पल्लवित व पुष्पित हुई। वे द्विवेदी जी को अपना काव्य गुरु मानते थे और उन्हीं के बताये मार्ग पर चलते रहे तथा जीवन के अंत तक साहित्य साधना में रत रहे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदलनों में भी भाग लिया और जेल यात्रा भी की।
जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं।
वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
पिताजी के आशीर्वाद से वह राष्ट्रकवि के सोपान तक पदासीन हुए। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि कहे जाने का गौरव प्रदान किया। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें दो बार राज्यसभा की सदस्यता प्रदान की। हिन्दी में मैथिलीशरण गुप्त की काव्य-साधना सदैव स्मरणीय रहेगी। बुंदेलखंड में जन्म लेने के कारण गुप्त जी बोलचाल में बुंदेलखंडी भाषा का ही प्रयोग करते थे। धोती और बंडी पहनकर माथे पर तिलक लगाकर संत के रूप में अपनी हवेली में बैठे रहा करते थे। उन्होंने अपनी साहित्यिक साधना से हिन्दी को समृद्ध किया। मैथिलीशरण गुप्त के जीवन में राष्ट्रीयता के भाव कूट-कूट कर भर गए थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओत प्रोत है। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम भक्त थे। परन्तु अंधविश्वासों और थोथे आदर्शों में उनका विश्वास नहीं था। वे भारतीय संस्कृति की नवीनतम रूप की कामना करते थे।
महाकाव्य
मैथिलीशरण जी की प्रसिद्धि का मूलाधार भारत–भारती है। भारत–भारती उन दिनों राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणापत्र बन गई थी। साकेत और जयभारत, दोनों महाकाव्य हैं। साकेत रामकथा पर आधारित है, किन्तु इसके केन्द्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। साकेत में कवि ने उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के हृदयस्पर्शी प्रसंग तथा उर्मिला की विरह दशा का अत्यन्त मार्मिक चित्रण किया है, साथ ही कैकेयी के पश्चात्ताप को दर्शाकर उसके चरित्र का मनोवैज्ञानिक एवं उज्ज्वल पक्ष प्रस्तुत किया है। यशोधरा में गौतम बुद्ध की मानिनी पत्नी यशोधरा केन्द्र में है। यशोधरा की मनःस्थितियों का मार्मिक अंकन इस काव्य में हुआ है। विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी केन्द्र में है। वस्तुतः गुप्त जी ने रबीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा बांग्ला भाषा में रचित 'काव्येर उपेक्षित नार्या' शीर्षक लेख से प्रेरणा प्राप्त कर अपने प्रबन्ध काव्यों में उपेक्षित, किन्तु महिमामयी नारियों की व्यथा–कथा को चित्रित किया और साथ ही उसमें आधुनिक चेतना के आयाम भी जोड़े।
भारत-भारती
'भारत-भारती', मैथिलीशरण गुप्तजी द्वारा स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है। भारतवर्ष के संक्षिप्त दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति 'भारत-भारती' निश्चित रूप से किसी शोध कार्य से कम नहीं है। गुप्तजी की सृजनता की दक्षता का परिचय देने वाली यह पुस्तक कई सामाजिक आयामों पर विचार करने को विवश करती है। यह सामग्री तीन भागों में बाँटी गयी है।
भारतवर्ष के दर्शन पर वे कहते हैं-
पाये प्रथम जिनसे जगत् ने दार्शनिक संवाद हैं-
गौतम, कपिल, जैमिनी, पतंजली, व्यास और कणाद है।
नीति पर उनके द्विपद ऐसे हैं-
सामान्य नीति समेत ऐसे राजनीतिक ग्रन्थ हैं-
संसार के हित जो प्रथम पुण्याचरण के पंथ हैं।
सूत्रग्रंथ के सन्दर्भ में ऋषियों के विद्वत्ता पर वे लिखते हैं-
उन ऋषि-गणों ने सूक्ष्मता से काम कितना है लिया,
आश्चर्य है, घट में उन्होंने सिन्धु को है भर दिया।
वर्तमान-खंड
दारिद्र्य, नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाते हुए, सामाजिक नूतनता की माँग रखी गयी है।
अपनी हुई आत्म-विस्मृति पर वे कहते हैं-
हम आज क्या से क्या हुए, भूले हुए हैं हम इसे,
है ध्यान अपने मान का, हममें बताओ अब किसे!
पूर्वज हमारे कौन थे, हमको नहीं यह ज्ञान भी,
है भार उनके नाम पर दो अंजली जल-दान भी।
नैतिक और धार्मिक पतन के लिए गुप्तजी ने उपदेशकों, संत-महंतों और ब्राह्मणों की निष्क्रियता और मिथ्या-व्यवहार को दोषी मान शब्द बाण चलाये हैं। इस तरह कविवर की लेखनी सामाजिक दुर्दशा के मुख्य कारणों को खोज उनके सुधार की माँग करती है। हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व की निष्क्रियता को उजागर करते हुए भी 'वर्तमान खंड' आशा की गाँठ को बाँधे रखती है।
भविष्यत्-खंडअपने ज्ञान, विवेक और विचारों की सीमा को छूते हुए राष्ट्रकवि ने समस्या समाधान के हल खोजने और लोगों से उसके के लिए आवाहन करने का भरसक प्रयास किया है।
राष्ट्रकवि
अपने साहित्यिक गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से गुप्त जी ने 'भारत-भारती' की रचना की। 'भारत-भारती' के प्रकाशन से ही गुप्त जी प्रकाश में आये। उसी समय से आपको 'राष्ट्रकवि' के नाम से अभिनंदित किया गया। उनकी साहित्य साधना सन् 1921 से सन् 1964 तक निरंतर आगे बढ़ती रही। गुप्त जी युग-प्रतिनिधि राष्ट्रीय कवि थे। इस अर्ध-शताब्दी की समस्त सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक हलचलों का प्रतिनिधित्व इनकी रचनाओं में मिल जाता है। इनके काव्य में राष्ट्र की वाणी मुखर हो उठी है। देश के समक्ष सबसे प्रमुख समस्या दासता से मुक्ति थी। गुप्त जी ने 'भारत-भारती' तथा अपनी अन्य रचनाओं के माध्यम से इस दिशा में प्रेरणा प्रदान की। इन्होंने अतीत गौरव का भाव जगाकर वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा दी। अपनी अभिलाषा अभिव्यक्त करते हुए वे कहते हैं-
"मानव-भवन में आर्यजन, जिसकी उतारें आरती।
भगवान् भारतवर्ष में, गूंजे हमारी भारती।"
प्रमुख कृतियाँ
'भारत–भारती' पुस्तक का आवरण पृष्ठ
मैथिलीशरण के नाटकों में 'अनघ' जातक कथा से सम्बद्ध बोधिसत्व की कथा पर आधारित पद्य में लिखा गया नाटक है।
प्रमुख कृतियाँ
- नाम प्रकाशित वर्ष
- जयद्रथ वध 1910
- भारत–भारती 1912
- पंचवटी 1925
- साकेत 1933
- यशोधरा 1932
- विष्णुप्रिया 1957
- झंकार 1929
- जयभारत 1952
- द्वापर 1936
- कुणाल गीत
- अजित
- अर्जन और विसर्जन
प्रमुख नाटक
मौलिक नाटक
अनघ
चरणदास
निष्क्रिय प्रतिरोध
विसर्जन
भास नाटक
स्वप्नवासवदत्ता
प्रतिमा
अभिषेक
अविमारक
गुप्त जी की 52 से भी अधिक काव्य रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ अनूदित भी हैं। उन्होंने 'मधुप' उपनाम से 'विरहणी ब्रजांगन', 'प्लासी का युद्ध' और 'मेघनाद वध' नामक बंगला काव्य कृतियों का अनुवाद किया है तथा कुछ संस्कृत नाटकों के अनुवाद भी किये। इसी प्रकार 'रुबाइयात उमरखय्याम' भी उमर खयाम की रुबाइयों का हिन्दी रूपान्तर है। इनकी उल्लेखनीय मौलिक रचनाओं की तालिका में- रंग में भंग, जयद्रथ वध, पद्य प्रबंध, भारत भारती, शकुंतला, तिलोत्तमा, चंद्रहास, पत्रावली, वैतालिका, किसान, अनघ, पंचवटी, स्वदेश संगीत, हिन्दू, विपथगा, शक्ति विकटभट, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, सिद्धराज, द्वापर, मंगलघट, नहुष, कुणालगीत , काबा और कर्बला, प्रदक्षिणा, जयभारत, विष्णुप्रिया आदि आते हैं।
पुरस्कार व सम्मान
मैथिलीशरण गुप्त हिन्दी के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि कहे जाते हैं। सन 1936 में इन्हें काकी में अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया गया था। इनकी साहित्य सेवाओं के उपलक्ष्य में आगरा विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इन्हें डी. लिट. की उपाधि से विभूषित भी किया। 1952 में गुप्त जी राज्य सभा के सदस्य मनोनीत हुए और 1954 में उन्हें 'पद्मभूषण' अलंकार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें हिन्दुस्तानी अकादमी पुरस्कार, 'साकेत' पर 'मंगला प्रसाद पारितोषिक' तथा 'साहित्य वाचस्पति' की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। 'हिन्दी कविता' के इतिहास में गुप्त जी का यह सबसे बड़ा योगदान है। 'साकेत' उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है।
मृत्यु
मैथिलीशरण गुप्त जी का देहावसान 12 दिसंबर, 1964 को चिरगांव में ही हुआ। इनके स्वर्गवास से हिन्दी साहित्य को जो क्षति पहुंची, उसकी पूर्ति संभव नहीं है।
झूठा-सच अखबार और jhuthasach.com की तरफ से मैथिलीशरण गुप्त जी के 58वीं पुण्यतिथि पर उन्हे नमन।








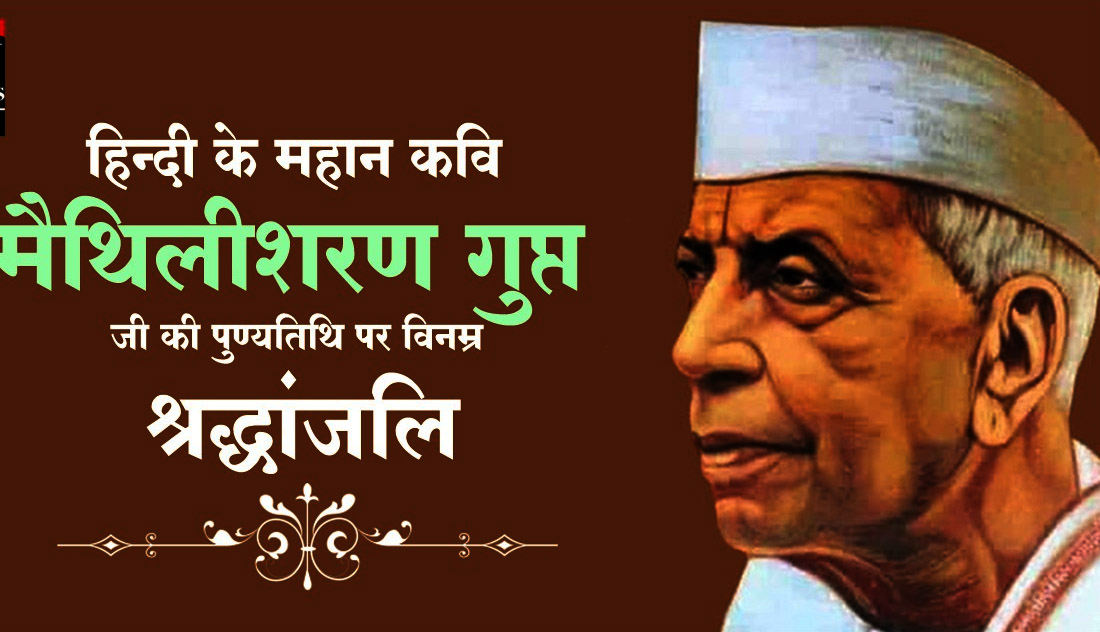
















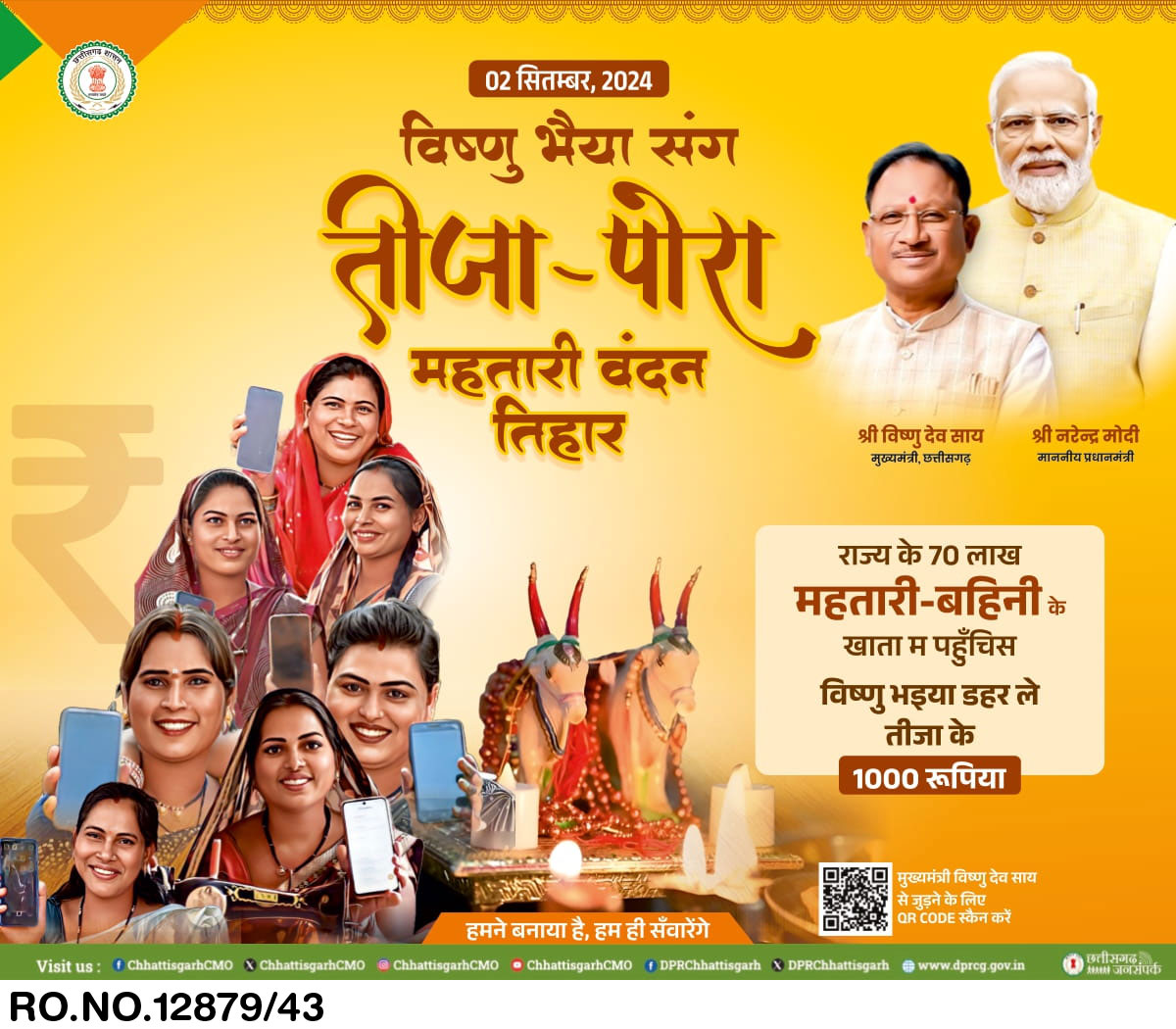




.jpeg)
.jpeg)